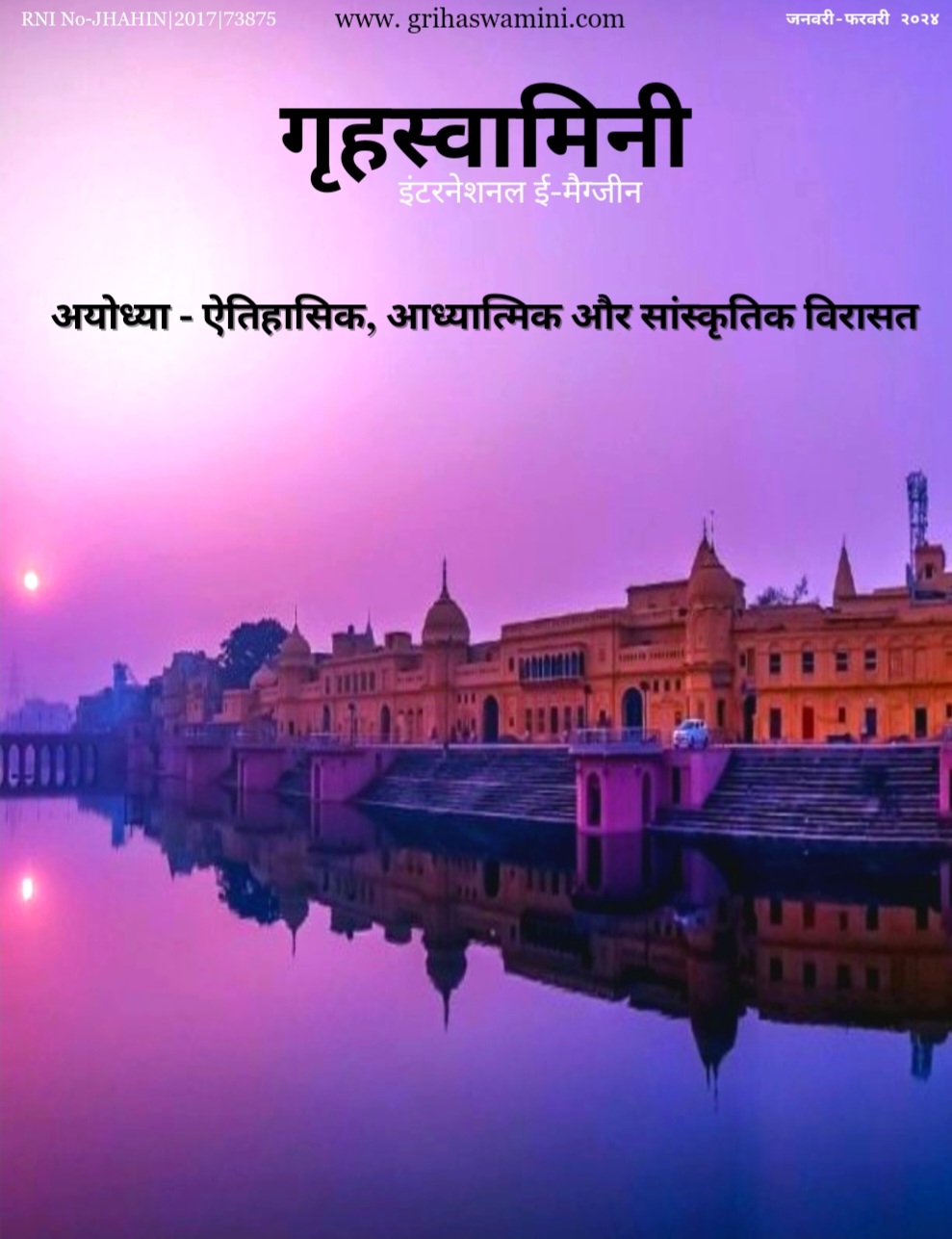साड़ी वाला दिन
लैक्टो-केलामाइन,बोरोलीन,केयो-कार्पिन जैसी माँ के जमाने की चीजों की तरह ही माँ और मां की पोशाक में भी कोई अंतर नहीं आता कभी, यही मैं समझती रही सदा, क्योंकि माँ को हमेशा साड़ी में ही देखा । हां ! थोड़ा सा बदलाव तब नजर आता जब वो बाहर जाने की अलग साड़ी पहनतीं ।
रसोई और अन्य घरेलू कामों के लिए प्रयुक्त होने वाली साड़ी बाहर पहने जाने वाली साड़ी से थोड़ा हल्की और भिन्न रहती । उसका फैब्रिक इन कामों में सुविधाजनक प्रतीत होता हो शायद । दादी और माँ उसे धोती कहते । उनकी धोतियां अलग-अलग मौकों पर हमारे लिए भी बहुत उपयोगी साबित होती थीं। सुबह जब माँ जबरदस्ती मुंह धुलाती तो हम गुस्से में उन्हीं के पल्लू से मुंह पोंछ लेते थे । खुश होते तो उसी पल्लू से कभी उनका मुंह ढ़ांपकर तो कभी अपना मुंह छुपाकर माँ के साथ खेलते । कभी किसी और के साथ छुप्पन-छुपाई खेल रहे हैं तो माँ को एक जगह खड़ा कर उनके पल्लू से छुपकर सोचते कि अब हम कहीं से नहीं दिख रहे । माँ भी सामने वाले को इशारा करती कि वो थोड़ी देर तक न ढ़ूंढ़ पाने का बहाना कर ले तो इसे भी छुपने में कामयाब रहने की संतुष्टि हो जाये । कभी ठंड में माँ से चिपककर जरा गरमी मिली तो उन्हीं की साड़ी का पल्लू ओढ़कर सो गये । हां,दोपहर में उनकी कोई दूसरी पूरी साड़ी हमें मिल जाती थी । वो साड़ी पहनकर बड़ी महिलाओं की तरह घरेलू काम करने का अभिनयपूर्ण खेल खेलते दोपहर बिताने का क्रम चलता रहता गर्मियों भर। मौसम आने-जाने के दोहराव में उम्र के अनुसार अब हम भी बच्चे से बडे़ हो रहे थे, तो मां भी प्रौढ़ावस्था की ओर जाती हीं । लकीरें यक़ीनन चेहरें में बदलाव लाती होंगी मगर पल्लू तो वही था, इसलिए मान के चले थे कि माँ कभी नहीं बदलती ।

ठगी सी रह गयी मैं, ससुराल में गेट खोलने पर एक दिन माँ को सामने खड़े पाया जब सलवार-सूट में ।
ये क्या ?? ??
माँ को अजनबीपन से प्रणाम किया । उन्होंने गले लगाया पर मैं लगी नहीं । माँ तो कुशल-क्षेम पूछ रही मगर मैंने जैसे मुंह में दही जमा लिया ।
अब माँ भी कुछ-कुछ समझ गयी । बोली- ” बुढ़ापा आ गया बेटा । साड़ी में ठंड लगती है तो तेरी भाभियों ने सलवार-सूट पहना दिया” ।
मैं माँ के लिए कुछ खाने के लिए ले आयी । वो खा ही रही थीं कि चम्मच उनके सूट पर उलट गयी । मैंने न उसे झाड़ने में जल्दी दिखायी और न पानी से साफ करने की कोशिश की । चुप बैठी रही । माँ बोली – “ये तो दाग पकड़ गया” । मैं खुश होकर अंदर भागी । हरे रंग की सितारे कढ़ी पल्लू वाली एक साड़ी लेकर आयी ।
” माँ! ये पहन लो। सूट मैं धुलवा कर भिजवा दूंगी” । माँ ने साड़ी पहन ली तो मेरा मन भी खिल गया जैसे । माँ, माँ सी जो दिखने लगी थी । अब मैं माँ से बहुत बातें करना चाहती थी, लेकिन माँ को जल्दी वापस जाना था । मैं उन्हें छोड़ने गेट तक गयी । दिल चाहता था देखती रहूं उन्हें देर तक । मगर उनका मन भी तो फिर लौट- लौट कर वापस आता रहेगा, यही सोचकर मैं भागकर अंदर चली गयी । ड्राइंगरूम की खिड़की से फिर देखती रही उन्हें जाते हुए जब तक आँखो से वो ओझल न हो गयीं । दूर तक, फिर देर तक लहराता रहा वो सितारों वाला आँचल आँखो के सामने।
प्रतिभा नैथानी
साहित्यकार
देहरादून, उत्तराखंड