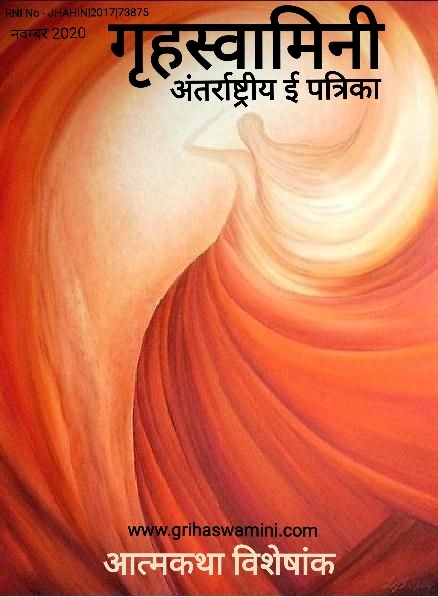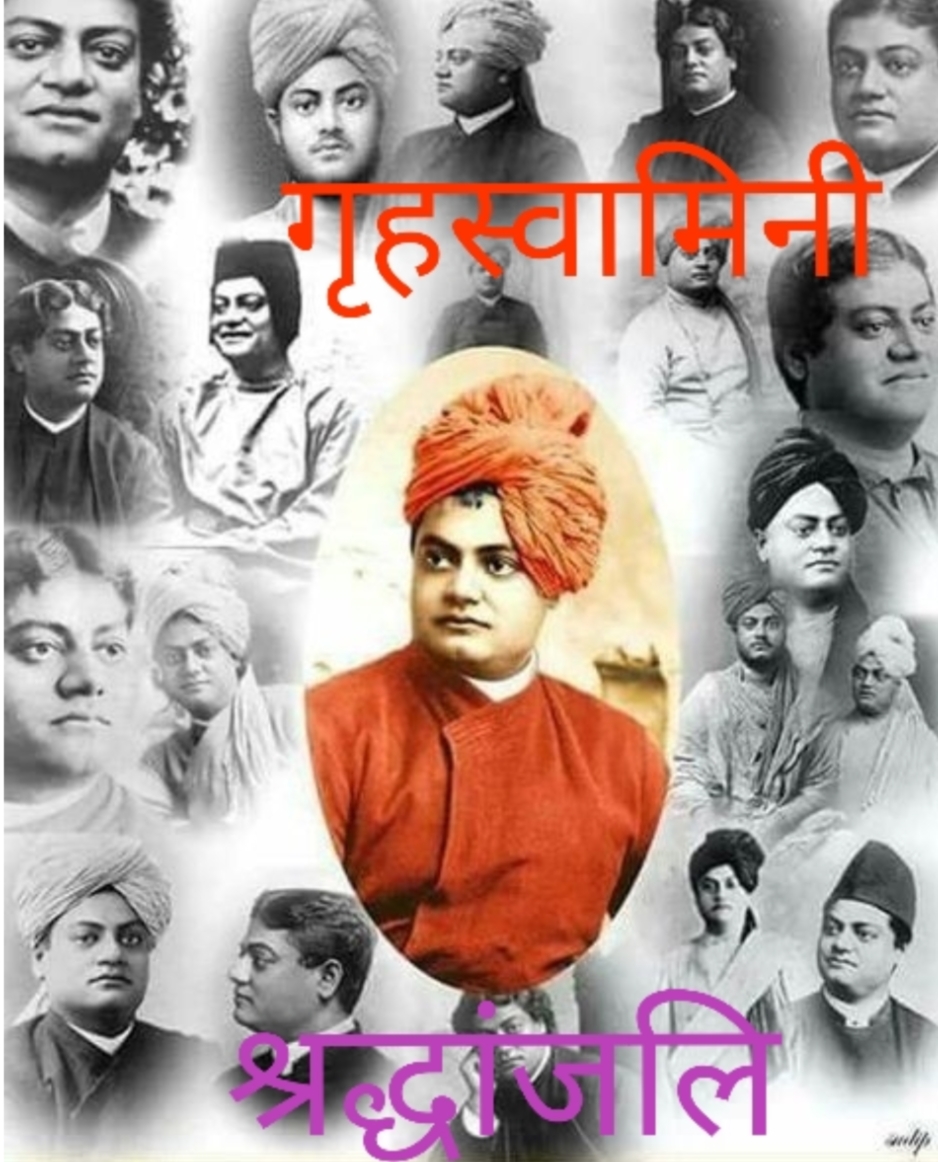ये तब नहीं समझा
मेरी दादी, जिन्हें हम ईया बुलाते थे
पाँच फीट से भी कम उनकी हाईट थी
पर किसी धोखे में न रहना
इच्छाशक्ति में वह बिल्कुल डायनामाइट थीं
लंबे वक्त से वैधव्य झेलते हुए
उस छोटी, बेहद दुबली सी काया में
कमाल की सेन्स ऑफ फाईट थी
बेटियों की शादी, इकलौते पुत्र की शिक्षा
उस अकेली, नाजुक सी जान ने ही निभाई थी
और अपने सारे दुख दर्द सीने में छुपा
परिवार में ही अपनी सारी शक्ति लगाई थी
माँ-पापा और हम चारों भाई-बहन
उनके जीवन की धुरी थे
उनकी अपनी भले ना हों
पर हमारी सारी जरूरतें पूरी थीं
सफेद, सूती साड़ी में लिपटी वह मूरत
गाँव में रहकर करती रही हमारी इच्छाओं की पूरत
और हमारे स्वार्थ ने कभी यह न जानना चाहा
कि क्या थी उनकी खुद की इच्छाओं की सूरत
शहर में रह रहे हम पोते-पोतियों के लिए
मनपसंद व्यंजन कभी बना भेजतीं
तो कभी अचार, पापड़, मुरब्बों के डब्बे सजा भेजतीं
(कसम से, उनके हाथ के ग्वाभा जैम और पेड़े लाजवाब थे)
हमने इन सबको बिलकुल फॉर ग्रांटेड लिया
मानों इसी के लिये तो वो एग्ज़िस्ट करती थीं
तब ये ना समझा, क्यों वो अक्सर हमें
गाँव आने को इन्सिस्ट करती थीं

हम गर्मी और सर्दी की छुट्टियाँ गाँव में बिता
अपनी ड्यूटी निभा दिया करते थे
मानों उनके ऊपर ही कोई
अहसान किया करते थे
फिर समय बीता, हम अपने-अपने गंतव्य को गए
हमारी ईया की ढलती उम्र के भी बुझने लगे दीए
जब अंत करीब आया तो प्रिय पुत्र को बुलाया
और अपने अंतिम शब्द “खाना खा लेना” चेताया
मतलब अपने अंतिम क्षणों में भी
अपने बच्चों की सुध लेती रहीं
कहीं वो भूखा ना रह जाये
यही परवाह करती रहीं
फिर छा गया अन्धकार
एक शून्य, बड़ा सा खालीपन
और तब ये अहसास हुआ
कि हमने क्या खोया
आख़िर ये कैसा व्यक्तित्व था!
खुद की नाहीं कोई इच्छा, ना गिला शिकवा
इतना त्याग!
और इतना निस्वार्थ भी जीता है कोई!
लेकिन अब समझी तुम महान थीं ईया!
ना सिर्फ उमर बल्कि अहसासों में भी
हमसे बहुत बड़ी, बहुत ऊँची थीं
जिसे हम चाहकर भी अब, कभी छू नहीं सकते
पर ये तब नहीं समझा…..
अफसोस, क्यों ये तब नहीं समझा!

रेखा सिंह
मुंबई, महाराष्ट्र