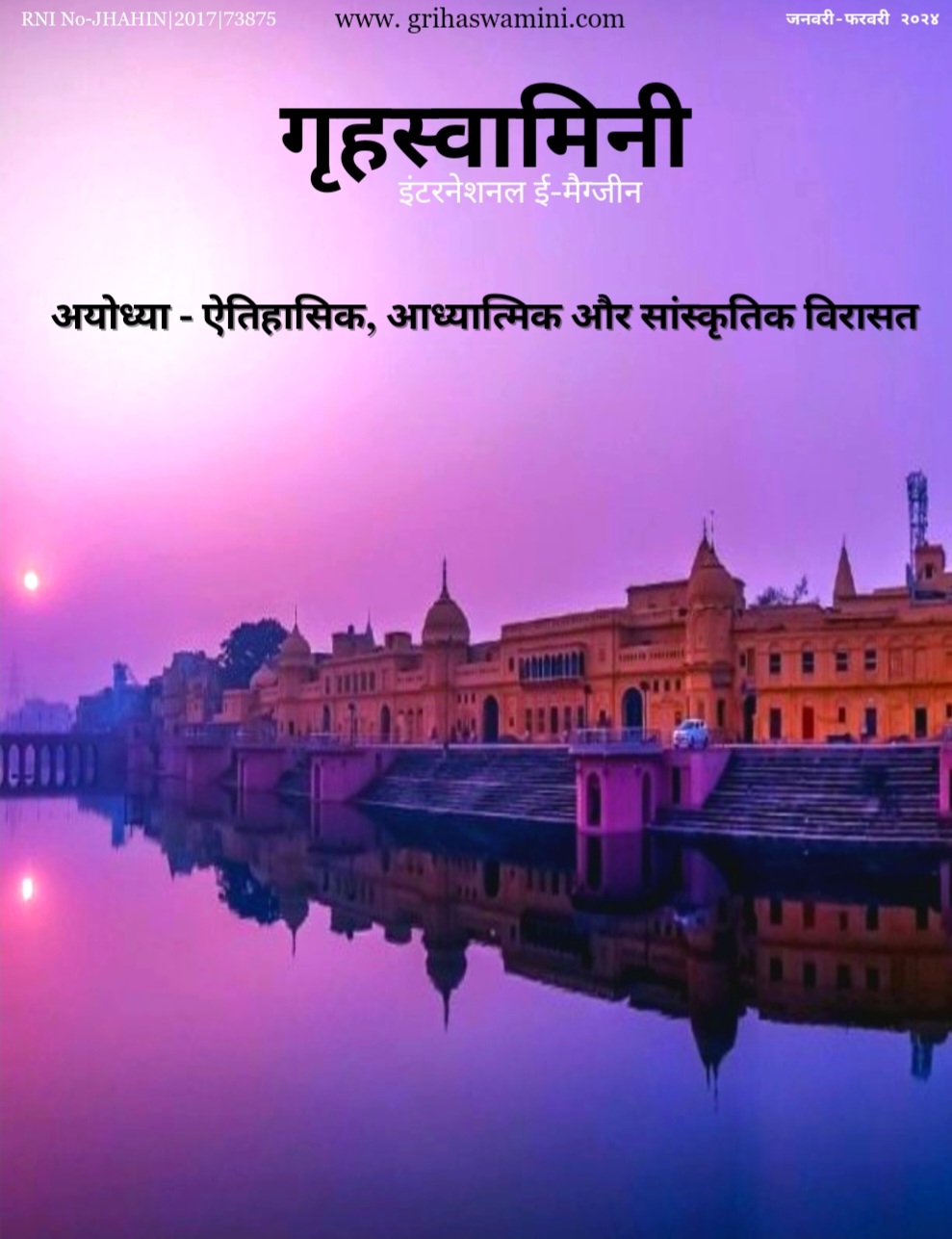दशहरा : भक्ति की विरासत
शिवरात्रि, होली, दीपावली, छठ – फिर बीच में तीज, सत्तुआनी, जितिया, भैया दूज – ये वर्ष के त्यौहार हैं बिहार के। कहने को तो बिहार एक भौगोलिक इकाई है लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बहुत फर्क है। कहते हैं ना, चार कोस पर बदले वाणी, ढाई कोस पर पानी – तो यहाँ भी ऐसा ही है। हर जगह के अलग स्वाद, रीति-रिवाज, खान-पान, तहज़ीब और संस्कार | पर्व मनाने के भी तरीके अलग हैं। भागलपुर में बंगाली संस्कृति की छाप है, मिथिलांचल में लोक परम्पराएँ हैं; पटना, मगध की राजधानी थी तो बोलचाल, पहनावा, संस्कृति मिल जुल गए हैं। ऐसे मिश्रित वातावरण में हम जब बड़े हो रहे थे तो ऐसा लगता था कि जीवन बस बेफ्रिकी है – सरल, संगीतमय, सुंदर – जो भी कमियाँ थीं, वो बड़े अपने में समेट लेते थे।
आज भी भागलपुर का दशहरा मुझे याद है। भागलपुर में दशहरा यानि कि “दस दिन हरा’ | हमारे घर में दस दिनों तक रोटियाँ नहीं बनती थीं – पूरी, कचौड़ी से मालामाल पेट पता नहीं कैसे सँम्हलता था।
पहली पूजा – दशहरे के पहले दिन, घर की बड़ी स्त्रियाँ तड़के उठती थीं। स्नान करके पूजाघर की सफाई, फर्श पर मिट्टी का लेपन, थाली-कलश – प्रसाद की तैयारी करती थीं और फिर पंडित जी का आगमन होता था। दादी, माँ, चाची का उपवास होता था आज के दिन। पंडित जी साधारणत: इन दिनों बड़ी पूछ में होते थे। उनके आने पर आसन ग्रहण करके फिर पूजा घर में मंत्रोच्चार कर कलश या ‘घट’ स्थापना होती थी। लाल कपड़े में नारियल लपेटकर, मिट्टी के कलश पर स्थापित किया जाता था। उसका स्थान होता था मिट्टी पर रखे हुए जौ पर | फिर सब बड़े, बच्चे भक्तिभाव से दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनते थे। पंडित जी का कंठ सुरीला था और वो गाते भी उच्च स्वर में थे। महिषासुर मर्दिनी, जगदम्बा, अम्बिका, कालिका देवी के नौ स्वरूपों में सिंह की सवारी किए हुए माँ दुर्गा सबसे लोकप्रिय हैं। पंडित जी का कार्यक्रम करीब डेढ़ घंटे का होता था। बच्चे इधर-उधर देखने लगते थे कि जल्दी शंख-घंटी बजे और पेट पूजा हो। कलश स्थापना दुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग था। पंडित जी के स्वर, शंख, मिली जुली बोलियाँ, आरती – ये सब बड़ी रीतियों के साथ किया जाता था। औरत दो जगहों की परम्पराएँ निभाती है। वह ‘उस’ घर में कुछ लेकर आती है और ‘इस’ घर की रीतियों को आगे बढ़ाती है। दबी-दबी आवाजें उठती रहती थीं – कलश पर स्वास्तिक बनाना है, सामने फूल रखो, पूजा की थाली नीचे ना रखो – इसी बहाने घर की औरतें अपनी बात कह देती थीं। फिर अगले पूरे नौ दिन तक “घट स्थापना” किए हुए कलश की सुबह-शाम आरती होती थी। सुबह की पूजा में देवी को उड़हुल का लाल फूल चढ़ाया जाता था। अपने से दुर्गा सप्तशती पढ़ने का इतना चलन नहीं था। शायद किताबें कम होती थीं या औरतों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। तब हम भी इतना नहीं सोचते थे। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी – ये चार दिन बहुत ही धमा-चौकड़ी से भरे होते थे। षष्ठी को माँ दुर्गा का मूर्ति स्वरूप अनावरण होता था। ढोल बाजे के साथ मूर्ति पंडालों में ले जाई जाती थी और बैठाई जाती थी। लाउडस्पीकर पर फिल्मी गाने बजते थे। भागलपुर में तब रातों को बड़ी धूम होती थी। हम लोग चार रिक्शों में लद॒कर मूर्ति दर्शन के लिए जाते थे। बंगाली पाड़ा के दर्शन में भोग मिलता था। नारियल दी हुई खिचड़ी। पहले ही 51 रुपए परिवार की तरफ से चले जाते थे – भोग के लिए। वो भोग की खिचड़ी किसी फाईव स्टार में भी ना मिले। इन दस दिनों में अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। गीले चावल को पीसकर “चौराठा” बनाया जाता था और उससे घर के दरवाजे, मंदिर के आगे छोटी-छोटी कलाकृतियाँ – रंगोली-बनाई जाती थी। ‘ऊँ लिखा जाता था। ऊँ घर से सभी विघ्नों को हटाने के लिए था। पूरे घर में इस चावल के घोल को छिड़का जाता था जिसे “अष्टमी जगाना’ कहते थे। बाद में इसको साफ करना भी कष्टदायक था | अष्टमी को कुछ स्त्रियाँ व्रत रखती थीं। पुरुषों को हमने केवल खाते ही देखा है। अष्टमी में बड़े पकवान बनते थे- पुलाव, पकौड़े, कचौरियाँ | बाहर से मिष्ठान आता था – जलेबी, गुलाब जामुन। घर में गुड़ डालकर गुलगुले भी बनते थे। हर दिन के खाने में अलग कुछ बनता था।
अष्टमी को फिर शाम में सब रिक्शे पर लद॒कर मूर्तियाँ देखने निकलते थे। देवी के भावों की, सजावट की खूब चर्चा होती | पंडाल के पास गोलगप्पे वालों की स्टॉल पर खाने की लाइन होती थी। पूरे तीन दिन नए कपड़े पहनते थे अष्टमी, नवमी और दशमी | कितनी तैयारियाँ चलती थी। होली, दशहरा में नए कपड़े पहनने का रिवाज है बिहार में। सुबह से गंजी, पजामों के साइड में पीली हल्दी लगाने की होड़ होती थी।
अष्टमी को सुबह ही पंडित जी फिर आते थे हवन करने के लिए। कहते हैं हवन के बिना पूजा अधूरी है। आज पंडित जी को नए कपड़े मिलेंगे। घर के नौकर-चाकरों को भी। और सब एक – दूसरे के लिए कुछ लाए हैं- साड़ियाँ, कपड़े, पेन और भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के साथ। हवन की सामग्री घर में ही बनती थी। पंडित जी के पिटारे से वो कुछ निकाल लाते थे – पीतल की थाली में गुड़ के साथ मिलाकर ऊँ और विभिन्न मंत्रों के साथ ‘स्वाहा’ की ध्वनी के साथ हवन होता था। संभवतः हवन होते हुए बारह बज जाते थे। तब तक सबको व्रत रखना होता था। जिसे भूख लगे, केला दूध खा लो।

अष्टमी, नवमी की गहमा-गहमी, खाना-पीना, खूब धमाचौकड़ी और गप्पे। घर की औरतें पैरों में लाल आलता लगाती, नई चूड़ियाँ बदलती और पहनती। चूड़ीवाली की टोकरी को सब घेरकर बैठ जाते। कुछ चुहल करने वाले मर्द भी। नवमी को बहुत घरों में सामिष भोजन बनता था क्योंकि नवमी को देवी को पशुओं की बलि पड़ती है। दुर्गा के मंदिरों में ये बलि का कार्यक्रम होता था। लेकिन हमारे यहाँ कलश बैठाने के कारण निरामिष आहार ही चलता था। शाम को शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। नाटक चलते थे। और रामलीला तो थी ही। शाम को विजयादशमी को कलश हिलाकर देवी को सांकेतिक विदाई दे दी जाती थी। एक अंतिम आरती होती थी। कलश के जल को पूरे घर में छिड़का जाता था। देवी रोग शोक से दूर रखे। नौ दिनों में जौ अंकुरित होकर “जैत” बन जाता था। सुंदर, हरा, जीवन का प्रतीक जैसे नया संदेश दे रहा हो। सब लोग एक दो अंकुरित जैत लेकर कानों में, बालों में खोंस लेते थे। यह देवी का आशीर्वाद था। बाद में किसी डिब्बे, किताब या पूजा स्थल में रख देते थे। इसके बाद बड़ों के पैर छुए जाते थे। बच्चों को, छोटों को -‘आशीर्वाद’ मिलता था। तब एक रुपया भी सौ के बराबर लगता था। इस “कमाई” को बच्चे बड़ी सुरक्षा से अपने माता-पिता से छुपा कर रखते थे। अब खाने की बारी थी। दहीबड़ा, पूए और पूरी, आलू की सब्जी, नारियल के लड्डू, कद्दू का पीली सरसों वाला रायता – अब इस खाने के स्वाद के लिए मन ललक जाता है।
शाम 4 बजे तैयार होकर बगल के पंडाल में चले जाते थे। घंटा, शंख, ढोल के बीच माँ दुर्गा की विदाई होती थी और संध्या समय बगल के तालाब में विर्सजन | प्रकृति का नियम अटूट है जो आएगा वो जाएगा भी। माँ दुर्गा की शक्ति श्रद्धा के साथ यह त्यौहार परिवारों को जोड़ने का भी काम करता था।
भागलपुर में रामलीला हर गली मुहल्ले में होती थी। रात में दस बजे तक बैठकर रामलीला देखते थे। हनुमान का लंका जलाना बहुत लोकप्रिय जो शायद रामलीला में छठे दिन आता था। रामलीला में जाकर प्लास्टिक के तीर धनुष लाना भी एक बड़ा आकर्षण था। वो तीर-धनुष अगले चार दिनों तक एक कौतुहल का विषय होते थे। शाम में फिर रामलीला मैदान में जाकर रावण का दहन देखना भी इस सिलसिले का अभिन्न अंग था। रावण, मेघनाथ और अहिरावण के पुतलों को जलते देखना अपने आप में अनुभव था। रामलीला के राम को आता देख लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते थे। दशहरा-दस दिनों का त्यौहार- देखते ही देखते खत्म हो जाता था। कलश का लाल कपड़ा पूजाघर में रख दिया जाता था सँम्हाल कर । हमारे यहाँ कन्या पूजन का उतना चलन नहीं था। मैं कोशिश करती हूँ कि परम्परा को आगे बढ़ाकर रखूँ।

-डॉ अमिता प्रसाद