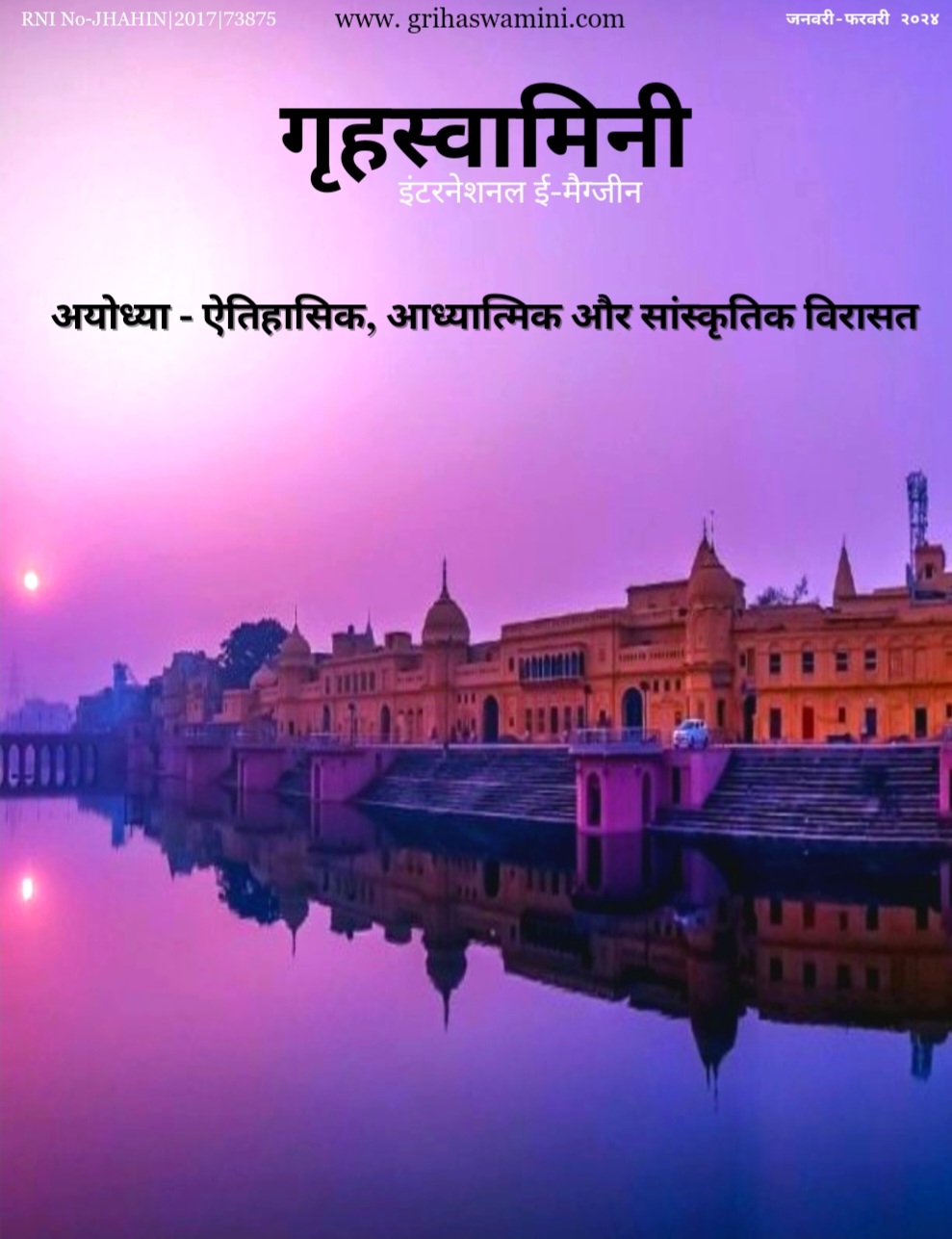भारत के मजबूर मजदूर
“चढ़ रही थी धूप,
गर्मियों के दिन,
दिवा का तमतमाता रूप,
उठी झुलसती हुई लू,
रूई ज्यों जलती हुई भू,
गर्द चिनगीं छा गयी,
प्रायः हुई दुपहर,
वह तोड़ती पत्थर..”
आप सबमें से कुछ लोगों ने महाकवि निराला की यह कविता सुनी होगी और मेरा दावा है जब भी आपने सुनी होगी आपका हृदय अवश्य द्रवित हुआ होगा और अगर नहीं भी द्रवित हुआ होगा तो भी आपने दुःखी होने का नाटक जरूर किया होगा…. पर मैं सच कहता हूँ मुझे उस पत्थर तोड़ती औरत को देखकर सुरक्षित सा महसूस होता है, उसका पत्थर तोड़ना मतलब किसी के पेट को भूख की आग से सुरक्षित रखना, किसी की अंतहीन रातों को, करवटों से सुरक्षित रखना… क्या कहा..?… “पर उपदेश कुशल बहुतेरो.. खुद इतनी मेहनत करनी पड़े तो पता चलेगा।”
तो मैं स्पष्ट कर दूं.. वह औरत कोई पराई नहीं मेरी अपनी ही माँ, बहन, पत्नी… नहीं… बेटी नहीं.. अभी वह पत्थर तोड़ने लायक बड़ी नहीं हुई है सो आप जैसों के घरों में वह क्या कहते हैं आपलोगों ने नाम दिया है.. याद आया ‘डोमेस्टिक हेल्प’ का काम करती है, वैसे कुछ अपेक्षाकृत जागरूक लोग उसके पढ़ाई – लिखाई की भी समुचित व्यवस्था कर देते हैं। आप समझ ही गयें होंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी… जी मैं भारत का एक मजबूर मजदूर हूँ… मेरी पहचान है चेहरे पर हल्की सी उदासी और आंखों में काम मिलने की आशा, वह मजदूर, जिसके पसीने मिली गारे और उसके हथौड़े से टूटी पत्थर और ईंट से आपके मजबूत इंडिया का नींव पड़ा है। वैसे तो हर वह व्यक्ति जो किसी सरकारी, गैरसरकारी या निजी प्रतिष्ठान में किसी के अधीन रहकर अपना जीविकोपार्जन करता है, मजदूर कहलाता है और 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की छुट्टी पाता है, परंतु सही मायने में मजदूर वह होता है जो केवल शारीरिक श्रम के बलबूते अपनी आजीविका कमाता है, जिसके पास न कोई विशेष प्रशिक्षण होता है न ही किसी श्रमिक संघ का वरद हस्त.. कहने का अर्थ कि मैं असंगठित क्षेत्र का मजदूर हूँ। हां मैं वह मजदूर हूँ जिसे कभी-कभी न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती और न काम के तय घंटों के विषय में बहस करने की औकात है मेरे पास, अपने मालिक, चाहे वह खेत का हो या किसी कल कारखाने का, की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। सुनते हैं कि उन्नीसवीं सदी में कोई कार्ल मार्क्स हुआ करते थे जिन्होंने नारा दिया दिया था कि, “दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ,तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने जंजीरों के।”
एक होना तो चाहते हैं साहब, लेकिन मजदूरी छोड़ने के शर्त पर नहीं… क्योंकि हमारे पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा भी बहुत कुछ है… रोटी है, बच्चों का लालन – पालन है, मां बाप का इलाज है। मैं और मेरे जैसे बहुत से मजदूरों का गांव घर छोड़ कर इन बड़े शहरों की ओर रुख करने के बहुत से कारण होतें हैं मसलन. कभी किसी अच्छे खासे किसान पर कर्ज का बोझ पड़ जाना, कभी हमारा पढ़ा – लिखा न होना, कभी शहर से आये अपने भाईयों दोस्तों के अच्छे पहनावे ओढ़ावे को देखकर प्रेरित होना, कभी गांव में उचित मजदूरी न मिलना, कभी घर में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने पर भूखमरी की नौबत आना और कभी एक बेहतर जिंदगी की खोज में मेट्रोपोलिटन शहरों में जाकर अपनी योग्यता के अनुसार किसी इमारत में राज मिस्त्री से लेकर ईंट ढोने तक का काम, कभी किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान, कभी घरेलू काम या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर अपनी जिंदगी चलाना। हमसे मिलने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, घर से निकले और वह देख रहे हैं न गैरेज उसमें हम हैं, रिंच पेचकस लिए, आप की गली के नुक्कड़ पर हैं, चाय और नाश्ता परोसते हुए, बर्तन धोते हुए, और वह जो आगे मेनरोड का चौराहा है, बहुत से शहरों में उसे लेबर चौराहा भी कहते हैं वहाँ पर तो हम बहुतायत में मिल जायेंगे, जवान, बूढ़ा, स्त्री, पुरूष.. सब, अपनी जरूरतों के अनुसार ले जाईए दिहाड़ी पर.. जिनका भाग्य अच्छा उन्हें तो काम मिल गया और जिनको नहीं मिला उनका भगवान मालिक.. इसीलिए मैं कहता हूँ कि पत्थर तोड़ती औरत देखकर हमें जिंदगी के प्रति एक आशा का भाव उत्पन्न होता है।
आजकल जब पूरा विश्व कोरोना के कहर से आक्रांत है, अमेरिका जैसे देश में हर रोज हजार की संख्या में लोग मर रहे हैं और भारत में भी इस बीमारी से पीड़ित होने वालों की संख्या स्थिर होने का नाम नहीं ले रही, आप ‘प्रवासी मजदूर’ शब्द बार – बार सुन रहे हैं और उसका मतलब भी जान ही रहें हैं, फिर भी जब मैं बताने बैठा हूँ तो मेरे मुंह से भी सुन लीजिए। प्रवासी मजदूर उन्हें कहते हैं जो दो वक्त की रोटी की जुगाड़ और एक तथाकथित अच्छे भविष्य के भ्रमजाल में कभी, अपने गांव – कस्बे से निकलकर पड़ोस के शहर में मजदूरी ढूंढने जातें हैं, जिनकी संख्या करीब आठ करोड़ है, और कभी तो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात जैसे जगहों तक चले जाते हैं और ऐसे मजदूरों की संख्या लगभग छः करोड़ है। यह करीब चौदह से लेकर पंद्रह करोड़ वह संख्या है जिनका पंजीकरण हुआ है नहीं तो वास्तविक संख्या तो पैंतालीस करोड़ के आसपास है, नीति आयोग की 2018 के रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 94 प्रतिशत कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करतें हैं, ऐसे कामगार किसी न किसी ठेकेदार या किसी संस्था के अधीन दैनिक मजदूर के तौर पर काम करतें हैं, जहां उनका भरपूर शोषण होता है आर्थिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर, और जहां भी थोड़ी चूं – चपड़ किये कि जो भी काम मिला उससे भी छुट्टी। लोग कहते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय में हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की 50 प्रतिशत भागीदारी होती है पर विडंबना तो देखिये खेत में फसल उगातें हैं हम, फिर भी पेट भर भोजन को तरसतें हैं, भवन अट्टालिकायें बनातें हैं हम और रहतें हैं नालियों के ऊपर बने छोटे – छोटे अंधेरे कमरों में, अस्पताल बनाते हैं हम पर हमारे इलाज के लिए उपलब्ध होतीं हैं कचरे और दुर्गंध से भरा दवाखाना जहां इलाज की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होती है, कार्ल मार्क्स ने सही ही कहा था, “पूंजी मृत श्रम है, जो पिशाच की तरह केवल जीवित श्रमिकों का खून चूस कर जिंदा रहता है और जितना अधिक वह जिंदा रहता है उतना ही अधिक श्रमिकों का खून चूसता है।”आप ही बताइए कि यह कहां का न्याय है कि मजदूर जिनके अर्थोपार्जन का आधार उनका शारीरिक श्रम है उन्हें इतनी मजदूरी भी ना मिले कि वह अपने परिवार के साथ एक पौष्टिक आहार तक ग्रहण कर सके। मशीनों के आगमन से श्रम की महत्ता और भी घट गई है, इसीलिए इस देश में भी पूंजी सस्ते श्रम का शोषण करती है, जबकि महात्मा गांधी तक ने देश को हिदायत दे दी थी कि, “उद्योग का महत्व इस बात से कतई नहीं आंका जाना चाहिए कि उससे दूर बैठी निष्क्रिय पूंजी भागीदारों को लाभांश कितना मिलता है, बल्कि इससे आंका जाना चाहिए कि इसमें लगे कामगारों के शरीर, प्राण और आत्मा पर उद्योग का क्या प्रभाव पड़ता है।” नेहरू जी भी इस संबंध में अच्छे खासे चिंतित हो कह उठे थे,” खेतों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है कि वह इतनी मजदूरी पाये कि अपना जीवन सुख सुविधा से बिता सके… ” पर अफसोस, ऐसा हो न सका।
इन सबके बावजूद भारत विश्व के मानचित्र पर अपनी मजबूत स्थिति बनाने में प्रयासरत रहा, अपना चंद्रयान, मंगलयान भेजना, सैटलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो या अंतरिक्ष पर रॉकेट प्रक्षेपण के क्षेत्र में सफलता के अलावा अन्य बहुत सारी योजनाओं की चमक दमक के आगे आजादी के बहत्तर साल के बाद भी हम मजबूत भारत के मजबूर मजदूर की वास्तविक स्थिति पर पर्दा डला था। ठीक वैसे ही जैसे कमरे के सारे कचरे के ऊपर से एक सुरुचिपूर्ण कालीन बिछा दिया गया हो। काश कि हम प्रवासी मजदूरों के, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन भी कहा जाता है सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार एक सम्मानजनक व्यवस्था पर कुछ कदम पहले से ही उठाई होती, और वह नहीं किया तो न सही अचानक की तालाबंदी तो न करती और इससे भी अच्छा होता कि यह कोरोना नाम की बीमारी ही नहीं होती, क्योंकि इसी बीमारी ने दुनिया के सामने भारत की इस कड़वी और बदसूरत सच्चाई के ऊपर से पर्दा उठाया है । पूरे देश में अचानक हुए लाक डाउन की घोषणा ने हमसे हमारी नौकरी और मजदूरी छीन ली,हमलोग तो अभी अभी होली मनाकर घर से लौटे थे सो हाथ भी खाली ही था, घर का किराया माफ भी हो जाये लेकिन पेट कैसे मानता, वह शहर जिसे हमने अपने खून पसीने से स्वर्ग सा बना दिया उसने हमें कुछ महीने बिना किसी चाकरी के अपने पास रखने का आश्वासन तक नहीं दिया, उसके लिए हम प्रवासी हो गये ..परदेसी हो गये वाह रे अखंड भारत वाह रे अनेकता में एकता वाला देश..। सो हम सब निकल पड़े अपने गांव की तरफ, पैदल, औरत, मर्द, बच्चे जवान.. अपने सामर्थ्य से ज्यादा बोझ लादे.. किसी को मुंबई से दरभंगा जाना था, किसी को नोयडा से बगोदर… जगह-जगह टीवी चैनल वाले हमलोगों को रोककर हाल चाल पूछ रहे थे.. माइक लेकर कैमरों पर बोल रहे थे, “यह जैसा कि आप देख सकते हैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां तक मेरी नजरें जातीं हैं प्रवासी मजदूरों का जत्था का जत्था पैदल ही निकल पड़ा है हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर अपने घर गांव तक पहुंचने के लिए, इनके लिए न कहीं खाने की व्यवस्था है न पानी की, बहुत तो नंगे पैर चल रहें हैं, कहीं-कहीं स्वयंसेवी संस्थाओं या स्थानीय प्रशासन द्वारा इनके लिए कुछ व्यवस्था जरूर की गयी है पर वह अपर्याप्त है… इस बदहाल, लूटे – पिटे सर्वहारा वर्ग के हुजूम को राजमार्ग पर निरंतर चलते हुए देख सन सैंतालीस में बंटवारे के शिकार लोग जो पैदल ही अपने लिए तय ठिकानों की ओर जाने के लिए मजबूर थे और जिस दृश्य को हम साहित्य, कला या फिल्मों के माध्यम से देखकर कई बार दहल चुकें हैं, वैसे दृश्यों की पुनरावृत्ति आज की तारीख में देखना दुःखद से ज्यादा शर्मनाक है.. गजलकार और कवि दुष्यंत कुमार ठीक ही कह गयें हमारे देश के विषय में,
‘बहुत मशहूर है आयें जरूर आप यहां,
यह मुल्क देखने लायक तो है हसीन नहीं’.. मैं… टी वी से… कैमरामैन… के साथ।”
हम सब आगे बढ़ गये, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर तय करना था, लेकिन अभी थोड़ी ही दूर गये थे कि पुलिस ने हमारा रास्ता रोक दिया.. यह एक नई मुसीबत.. फिर हमने इसका भी तोड़ ढूंढा.. दिन भर वहीं किसी पेड़ की छांव में आराम करेंगे और रात के ठंडे मौसम में रेलवे पटरी के साथ – साथ आगे बढ़ेंगे। योजनानुसार रात भर सफर कर पांच बजे सुबह हमलोग जिस जगह पहुंचे वहां एक हृदयविदारक दृश्य से सामना हुआ, सत्रह मजदूर जो शायद थककर इन्हीं पटरियों पर सो गए थे, एक मालगाड़ी उन्हें कुचलती हुई निकल गई थी,क्या कसूर था इनका ये रोटी के लिए ही तो घर जाना चाहते थे, फिर क्यों मारे गए, इन्होंने कोई जुलूस भी तो नही निकाला था जैसा कि 12 जनवरी 1944 को ग्वालियर के मजदूरों ने निकाला और उस पर गोलियां चलाई गईं और कवि शमशेर बहादुर सिंह चीत्कार उठे थे,
“गरीब के हृदय
टंगे हुए,
कि रोटियां लिए हुए निशान,
लाल – लाल
जा रहे
कि चल रहा
लहू भरे गवालियर के बाजार में
जुलूस
जल रहा
धुआं धुआं
गवालियर के मजूर का हृदय”
और इन्होंने तो अपनी रोटियों का प्रबंध भी खुद कर रखा था।
खैर ऐसे ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए हमलोग गांव की सीमा तक पहुंचें, एक विद्यालय में चौदह दिन तक क्वारैंनटाईन होने के बाद कल अपने घर पहुंचे।… अब क्या करेंगे.. मनरेगा के तहत काम करेंगे… ना.. ना अब वापस नहीं जायेंगे गजलकार दुष्यंत कुमार सही ही कह गये,
“सोचा था उनके देश में मंहगी है जिंदगी,
पर जिंदगी का भाव वहां और भी खराब”
… नहीं साहब अब तक मेहनत की खायें हैं अब चोरी चकारी थोड़े करेंगे.. नक्सली बनकर खून खराबा करने से भी किसी का भला नहीं होने वाला… हां आंदोलन हो सकता है क्योंकि,
” पक गई हैं आदतें बातों से सर होंगी नहीं,
कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं” (दुष्यंत कुमार)
उससे भी बढ़िया एक बात, क्यों नहीं हम अपने देस में भी वैसा कुछ करें जैसा आज से डेढ़ सौ साल पहले गये गिरमिटिया मजदूरों ने मॉरीशस में जाकर किया.. उसे एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर देश बनाकर..। हम भी अपने प्रदेश में ही आत्मनिर्भर हो कर…। क्यों नहीं संभव है..?
“कौन कहता है आसमान में सूराख नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों।”
इस कोरोना ने हमें अपने गांव अपने देस का मूल्य बता दिया है।
ऋचा वर्मा
साहित्यकार
पटना, बिहार