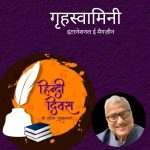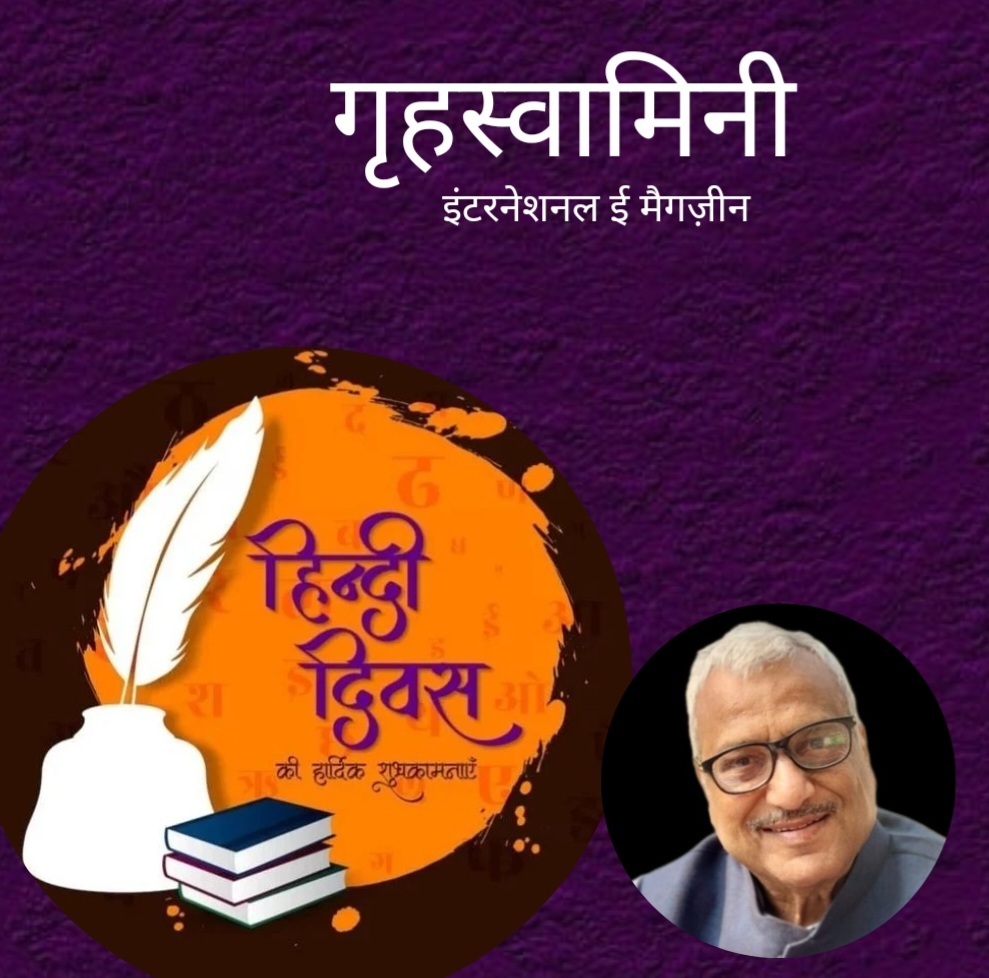घर से चलकर पूरी दुनिया तक की यात्रा हैं – दिव्या की कहानियाँ
चुनिंदा कथाकार ऐसे होते हैं जो शून्य से शुरू तो होते हैं किन्तु वे किस हद तक चले जाएंगे, इस बारे में कयास लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। हिंदी साहित्य की पहली और दूसरी पीढ़ियों के कथाकारों और यहाँ तक कि मंझे हुए कथाकारों में भी, स्थैतिकता और ठहराव है जहाँ वे स्वयं को स्वयं द्वारा बुने गए कथानकों के एक निश्चित दायरे तक ही सीमाबद्ध रख पाते हैं और अपने चिंतन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। समीक्षकों की नई पीढ़ियां रचनाकारों को अपने समय के चश्में से बड़े आकार-प्रकार में देखना चाहती हैं तथा उनके रचना-संसार को ठिंगना न बनाते हुए एक नई दिशा प्रदान करती हैं। बहरहाल, हिंदी साहित्य की अद्यतन पीढ़ी की कथाकार दिव्या माथुर की कहानियों में ऐसी कोई बात नहीं है कि बाल की खाल निकालते हुए उनमें क्षितिज के पार, चतुर्दिक देखने की कोशिश की जाए। अगर यह छोर दिखता है तो उस छोर को भी देखा जा सकता है। हाँ, बड़ी सहजता और सायसता से। बिलाशक, उनकी कहानियों में पात्रों की जटिल मानसिकता तो है; पर, सुस्पष्ट कथानक के ताने-बाने के साथ जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता है, वह उनके पात्रों की जटिल मानसकिता को समझने के लिए बहुत आसान बना देता है। उल्लेख्य है कि दिव्या को अपना कथानक बुनते हुए यह भली-भांति पता होता है कि उसका आकार-प्रकार कैसा होगा और एक कथाकार के लिए ऐसा होना आवश्यक भी है; तभी वह अपने विचार-तत्त्व को पुष्ट बना सकेगा और अपने कथ्य के चरम उद्देश्य को सहजता से स्थापित कर पाएगा। इस प्रयोजनार्थ वह कहानी के हर औजार का इस्तेमाल बड़ी सूझबूझ के साथ करती हैं। यदि ऐसा कहा जाए कि दिव्या ने इस संसार के दोनों गोलार्धों को अपने आनुभविक स्तर पर देखते-भोगते हुए अपने कथा-संसार को व्यापक स्वरूप प्रदान किया है तो यह संपूर्ण सच नहीं है क्योंकि नई दुनिया और पुरानी दुनिया से कहीं अधिक व्यापक और अपरिमेय होती है – मनुष्य की मानसिक दुनिया जिसमें दिव्या सतत यात्रा करती हुई नज़र आती हैं। यदि वह ब्रिटेन-प्रवास नहीं करती तो भी उनके सामाजिक वीक्षण-अनुवीक्षण का दायरा व्यापक होता क्योंकि उनके दृष्टिकोण में मानव-जीवन का हर पक्ष, अपने समस्त उपांगों समेत शामिल होता है। उनकी कहानियों में पूर्व-पश्चिम की ज़िन्दगियों की टकराहट की ध्वनियाँ-प्रतिध्वनियां, गूँज-अनुगूँज स्पष्टतया श्रव्य-दृष्टव्य हैं।
दिव्या की कहानियों में केवल ‘ओरिएंटल’ (oriental) और ‘ऑक्सीडेंटल’ (occidental) संस्कृतियों और परंपराओं की टकराहट की टंकार ही नहीं सुनाई देती है, अपितु विलिंगियों के बीच की तीखी नोकझोंक के दहकते तेवर मर्म-स्थल तक को पिघला जाते हैं। इन विलिंगियो के माध्यम से भी दिव्या पौर्वात्य और पाश्चात्य संस्कृतियों के बीच की टकराहट को बिंबित करती हैं।
लिंग-वर्ग-जाति आधारित दलित चिंतन, वामी विचारधारा और आधी दुनिया को पोषित करने वाला स्त्री-चिंतन ऐसी संकरी गलियां हैं जहाँ से गुजरते हुए दिव्या चुटहिल हो जाती हैं और तब वह झट से इन गलियों का परित्याग करते हुए जीवन के एक अत्यंत चौरस और खुले मार्ग पर आ जाती हैं जहाँ उन्हें सिर्फ मानव का दर्द और कराह तथा मानव-जीवन में अभावों का ठूंठ मंज़र नज़र आता है; कुंठा और संत्रास दिखाई देता है। उन्हें यह बिलकुल नहीं दिखता कि दर्द से कराहते मनुष्य का वर्ग, जाति या लिंग क्या है; व्याधियां भौगोलिक या राजनीतिक सीमाएं नहीं पहचानती। वे सार्वभौमिक होती हैं। सतत मानवीय चिंतन का उनका स्वभाव उनके कथानकों को इतना खाद-पानी देकर उनकी रचनाधर्मिता को उर्वर बनाता है कि उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता पाठकों को विस्मित करती जाती है।
दिव्या की भारतीयता से अविलगेय आत्मीयता है; फिर, उनके आचार-विचार का प्रतिनिधित्व करने वाली उनकी पात्र क्यों न हों?दिव्या की कहानियां बहिर्मुखी और बहुमुखी होती हैं।उन्हें विभिन्न कोणों से जांचिए-परखिए, यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो संवाद या कथोपकथन पात्रों की ज़बान से फूटे हैं, वे नपे-तुले हैं; जितने पात्र उनकी किसी कहानी में चित्रित हैं,वे आवश्यकतानुसार हैं;जिस क्रिया-व्यापार में पात्रों को डाला गया है, वह उनके समाज के अनुकूल हैं। अस्तु, बहुत-प्राय: पाठक को यह आपत्तिजनक लगता है कि दिव्या अपने विचार-संप्रेषण में इतनी विस्फोटक क्यों हैं और यहाँ तक कि यौन चेष्टाओं के आपत्तिजनक प्रतिरूपों को भी इतने कर्णस्फोटक लहजे में फटकार क्यों लगाती हैं। यह आवश्यक भी है क्योंकि दिव्या का ध्यान कहानी-कला के सभी छह औज़ारों पर केंद्रित होता है; किसी औजार को छोड़ें तो कैसे छोड़ें! एक वीरांगना-कथाकार तो अपने सभी छह सैनिकों के साथ, शब्द-सारथी की सहमति में, संप्रेषण के चौरस मैदान में छककर लड़ना चाहेगा। सो, दिव्या लड़ती हैं, लड़ती ही जाती हैं।
डॉ मनोज मोक्षेन्द्र, भारतीय संसद में संयुक्त निदेशक, ‘वी विटनेस’ पत्रिका और न्यूज़ पोर्टल के सलाहकार और संपादक, की डेढ़ दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं; प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशित होते रहते हैं।
डॉ मनोज मोक्षेंद्र
भारत