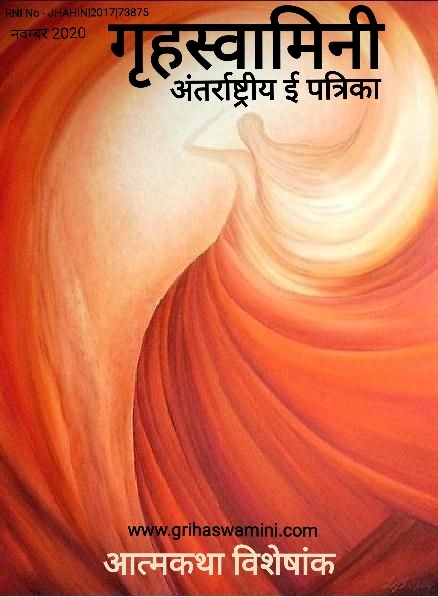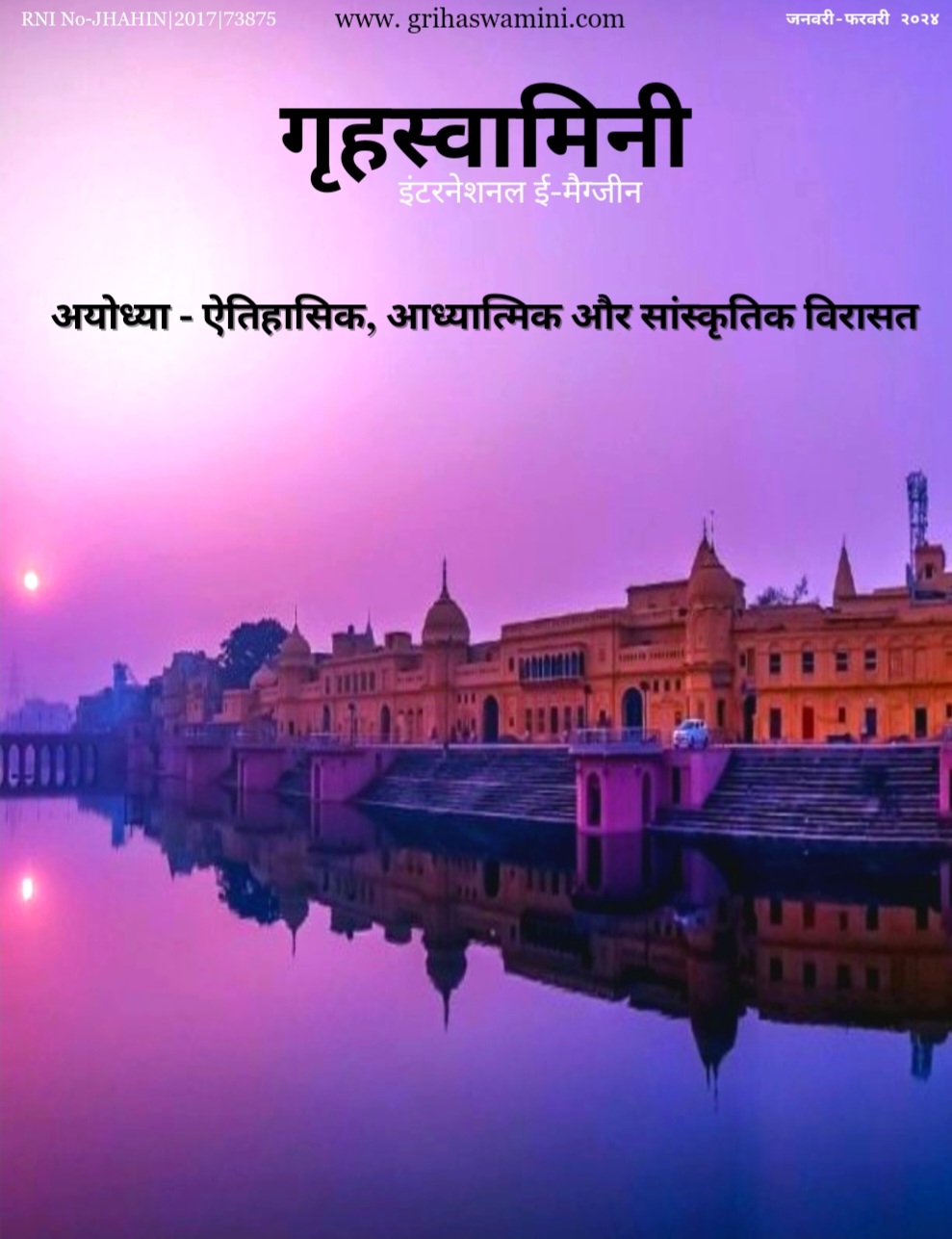बचपन: उजला पक्ष
उम्र के इस पड़ाव पर बचपन याद करना अच्छा लग रहा है। मेरा जन्म अपने बाबा के घर गोरखपुर में हुआ। हमारे बचपन में घर में खाने-पीने की सामग्री भरपूर होती थी मसलन दाल-चावल, आटा, दूध-दही मगर सजावट या प्रदर्शन के नाम पर कुछ नहीं था। हम बहुत अमीर नहीं थे पर गरीबी का अहसास न था। खाते-पीते और मस्त रहते। घर में फ़र्नीचर के नाम पर एक-दो तखत, चार-पाँच चारपाई, एकाध मेज और लकड़ी की दो कुर्सियाँ थीं। बाबा की कुछ किताबें जिसमें राहुल सांकृत्यायन की उनकी प्रिय किताब ‘वोल्गा से गंगा’ भी थी। रात को चारपाइयाँ बिछ जाती। सर्दियों में उन पर गद्दे-चादर बिछ जाते, रजाइयाँ निकल आतीं, गर्मियों में केवल चादर। तखत वैसे ही रहते, केवल बिस्तर लपेट दिया जाता। सुबह सबसे पहला काम होता बिस्तर लपेट कर चारपाई खड़ी कर देना। दोपहर को यही खड़ी चारपाइयाँ ऊपर से चादर डाल कर बच्चों के खेल घर होतीं। उसी में कोई बाबा बन कर मिल जाता कोई लोचन बन उनका नाश्ता ले जाता। कोई दादी रसोई तैयार करती। कोई माताजी बच्चों को दूध पिला रही होतीं। कोई बुआ बन स्वेटर बुन रही होती। कोई टीचर बन बच्चों को पढ़ाता। टीचर बनने का मतलब था हाथ में छड़ी।
गर्मियों में शाम होते आँगन में पानी का छिड़काव होता, आंगन पक्का था तो कई बार धुलता भी और खाटें आंगन में निकल आती। कभी रात को बूँदाबाँदी हुई तो पहले गुड़ीमुड़ी पड़े रहते वर्षा के रुकने का इंतजार करते यदि तेज हो गई तो भीतर कमरों में भागते। भागते हुए खाट उठाना नहीं भूलते। एक खाट पर दो-तीन बच्चे आराम से एक-दूसरे से सट कर सोते और सोने के पहले खूब लड़ना-झगड़ना, चिकोटी काटना, बकोटना चलता। ज्यादा ऊधम करने पर बड़ों से कनैठी, थप्पड़ आम बात थी। रोना-सुबकना भी। फ़िर कुछ देर बाद बच्चे पूर्वावस्था में आ जाते। डाँट-मार का बहुत असर नहीं होता था। माताजी ने डाँटा तो रो कर बाबा के पास चले गए, ताऊजी गोद में उठा कर बाहर घुमाने ले जाते। बुआ पुचकारने लगती तो कभी दादी माताजी को डाँट देती और हम चुप हो जाते।
दरवाजे पर एक आम का पेड़ था जिसे बाबा ने लगाया था। रात को आँधी चलने पर दादी बच्चों के साथ टिकोरे या आम बटोरने निकलती, सारे लोग निकल आते। बटोरने की होड़ लगती कोशिश होते हमारे आम कोई और न चुन पाए। हमारी छोटी बुआ बहुत शरारती थीं। जब कभी डाँट-मार की नौबत आती सर्र से इसी आम के पेड़ पर चढ़ जाती। बड़ी बुआ, बीच वाली बुआ, दादी नीचे खड़ी खीजतीं। दादी हार कर कहती, ‘आने दे तेरे पिताजी को।’ इस बुआ को बच्चों से बहुत लगाव था। मोहल्ले के किसी भी बच्चे को उठा कर ले आती और खिलाती। एक बार एक स्त्री ने अपना बच्चा ले जाने का बुरा माना तो उसका बच्चा लेकर पेड़ पर चढ़ गई। बच्चे की माँ की साँस ऊपर-की-ऊपर, नीचे-की-नीचे। पेड़ के नीचे खड़ी बड़ी मिन्नते करती रही। फ़िर जब मन भर गया तो बुआ बच्चा ले कर नीचे उतरी और उस औरत को उसका बच्चा पकड़ा दिया ऐसा दिखाया मानो कुछ हुआ ही न हो। मेरे पिताजी दूसरे शहर में काम करते थे। पहले हॉस्टल में रह कर पढ़ते थे। जब घर आते तो खूब रुआब रहता। तीनों बुआ उनसे खूब डरती थीं। एक बार इस छोटी बुआ को पिताजी ने डाँटा। तब वे कुछ न बोलीं लेकिन जब पिताजी चले गए तो हैंगर में टँगे उनके पैंट की छड़ी से खूब पिटाई की। आज तीनों बुआ, चाचा, माताजी-पिताजी सब जा चुके हैं। बाबा-दादी भी।

गिरने पर रोते तो बड़े कहते अरे देखो फ़र्श टूट गया। चोट पर कोई बड़ा फ़ूँक मारता तो रोना रुकता। नजर लगने पर – जो हर दूसरे-तीसरे दिन लगा करती थी तो लोटे में पानी ले कर न्योछ दिया जाता और पनारे पर लोटा उलटा दिया जाता या नमक-मिर्च न्योछ कर आग में डाल दी जाती। कभी-कभी फ़िटकरी न्योछ कर अंगारों पर रखी जाती और उसमें नजर लगाने वाले का चेहरा देखा जाता जिसकी शकल किसी-न-किसी से अवश्य मिलती। नजर लगने का मतलब था, बच्चे के शरीर में हराहट, भौंहों का ऊपर चढ़ जाना, उसका सुस्त पड़ जाना, शैतानियाँ करना बंद कर देना। जब मामला गंभीर लगता, बाबा के सहकर्मी-दोस्त मौलवी साहब बुलाए जाते। वे कुछ बुदबुदाते, मोरपंख से बला उतारते और अगले दिन बच्चा फ़िर अपनी बदमाशियों पर उतर आता। डॉक्टर की जरूरत शायद ही पड़ती। वैसे बाबा के दोस्त एक डॉक्टर थे जो रात-बिरात जब बुलाओ हाजिर हो जाते थे।जरूरत पर सिविल सर्जन भी घर आ जाते थे।
त्योहारों में खूब मस्ती रहती क्योंकि उस दिन डाँट-मार नहीं पड़ती चाहे कितनी शैतानी करो। दशहरे के कई दिन पहले से दादी-बुआ-माताजी नमकीन सेव, बूँदी के लड्डु, शकरपारे बनाती जिन्हें कनस्तर में भर कर भंडारघर में रखा जाता। होली के पहले गुजिया बनती। मुश्किल थी पूजा के पहले इन्हें खाना मना होता था। दिवाली वाले दिन खीर बनती। बेसब्री से पूजा खतम होने का इंतजार किया जाता। पूजा खतम होते भुक्खड़ों की तरह हम मिठाई पर टूट पड़ते। कई दिन तक केवल मिठाई से पेट भरा जाता कई बार चुरा कर भी खाते। फ़ुलझड़ी, अनार और दीवाल बम, चुटपुटिया फ़ोड़ते। दशहरे-दिवाली और होली पर नए कपड़े बनते। साल में दो बार नए कपड़े मिलते। बाबा और नाना जी थान खरीदते और सब बच्चों का नाप लिया जाता। एक छीट की सबकी फ़्रॉक और कमीज बनती। बाकी समय बड़े बच्चों की उतरन पर छोटे बच्चे मगन रहते। इस बात को ले कर नाक-भौं चढ़ाई जा सकती है यह मालूम न था। हमारी एक मौसेरी मौसी का कोट बना। जब उनको छोटा हो गया तो मुझे मिला, कुछ साल बाद उसे मेरी छोटी बहन पहनने लगी। बच्चों के कपड़े थोड़ी बड़ी नाप के बनाए जाते थे ताकि अगले साल तक पहन सकें, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बच्चों की अपनी पसंद-नापसंद जैसी कोई कल्पना न थी।

रात में हम बच्चों का एक भोजन था। दूध में मीड़ी हुई रोटी। बेला में दूध-चीनी में रोटी के टुकड़े करके मसल दिए जाते। बेला फ़ूल-काँसे का कम ऊँचाई का कटोरानुमा छोटी थाली होती थी। मौसेरा भाई दूध-रोटी खा उसी बरतन में थोड़ा पानी डाल कर पी लेता था जो मुझे बड़ा अजीब लगता था। दिन में दो बच्चों को एक थाली में खाना मिलता। थाली में एक किनारे चावल/रोटी होती, दूसरी ओर घी पड़ी दाल और थोड़ी-सी सब्जी। खाना शुरु करने पर हम पसंददीदा चीज पर सबसे पहले हाथ साफ़ करते और जब पेट-हिक भर जाती तो दूसरे की ओर बचा खाना ढ़केलते, कहते, देखो यह नहीं खा रहा/रही है। खाना थाली में छोड़ना मना था और एक दाना बाहर गिराना भी। बड़ों को चाय पीते देख तरसते थे। रात को बिना दूध रोटी खाए या दूध पीए मुझे नींद नहीं आती थी। इसी से जुड़ा एक मजेदार वायका सुनाती हूँ।

दादी मुझे और मुझसे साढ़े तीन साल बड़े चाचा को ले कर अपनी बहन से मिलने उनके गाँव गई। अलीगढ़ के पास का कोई गाँव था। उनकी बहन अकेली रहती थीं। गोरखपुर में हमारे दरवाजे पर सदा गाय रही और हाथरस के बरामई गाँव में गाय और भैंस दोनों। दादी की बहन के आँगन में भी गाय थी। रात को मुझे दूध नहीं मिला। दादी मुझे और चाचा को ले कर सोई बगल वाली खाट पर उनकी बहन सो रही थीं। दोनों बहनें बतिया रही थीं। मैंने कुड़मुड़ाना शुरु किया। मुझे नींद न आए। दादी ने पूछा, ‘क्या हुआ सो च्यों नहीं रही है?’ तब मैंने कहा, ‘नींद कहती है, दूध दो नहीं तो मैं नहीं आऊँगी।’ सुन कर उनकी बहन बहुत परेशान हो गई। दादी ने कहा दूध नहीं है। मैं रोने लगी और बोली तुम झूठ बोलती हो गाय तो है। उन्होंने कहा गाय बिसुख गई है। मेरी समझ में कुछ न आया मैं रोती रही। गाँव में साँझ पड़े सोता पड़ जाता है। मगर दादी की बहन गई, किसी से माँग कर दूध लाई, चूल्हा जला कर गरम किया, मुझे दिया और तब जा कर मैं सोई। काफ़ी दिन तक सब मुझे चिढ़ाते रहे, ‘नींद कहती है, दूध दो नहीं तो मैं नहीं आओँगी।’
पिताजी दूसरे शहर में काम करते थे। जब माताजी उनके पास रहने गई तो मेरे बाद वाली बहन छोटी थी। सोचा गया बहु दो बच्चों को कैसे संभालेगी? अत: बहन दादी के पास रह गई क्योंकि मैं माताजी को छोड़ने को तैयार न थी और मुझे माताजी की भेदिया माना जाता था, जो दादी-बुआ की बातें माताजी को बताया करती थी। मैं बहन की तरह सुंदर भी न थी, वह दादी-बुआ की लाड़ली थी। इस सुंदर बहन के लिए बुआ ने लाल मखमल (शनील नहीं) की फ़्राक बनाई, हाथी आया था उस पर बैठा कर घुमाया गया। शाम को उसे तेज बुखार था, नजर लग गई थी। जब उसके बाद भाई हुआ तो कुछ दिन बाद वह भी उन्हीं लोगों के पास रहने लगा। मैं माताजी से चिपकी रही। फ़िर एक और भाई हुआ। वही भाई जो इस साल गुजर गया। यह भाई शुरु से बहुत तेज दिमाग और स्वभाव से बहुत शरारती था।
देवबंद में शाह बुल्लन की गली के घर का हमारा आँगन बहुत बड़ा था बीसियों खाट बिछ सकती थी। गर्मियों में शाम को पानी का छिड़काव होता, रात खुले आसमान के नीचे सोते। एक दिन रात में किसी को सिरदर्द था सो उसने पेनबॉम लगाया। सुबह सब अपने काम में लग गए। यह भाई छोटा था अभी चलना सीख रहा था। उठ कर बैठा सामने पेनबॉम की शीशी दीखी जाने कैसे खोल कर आँख में काजल की तरह भर लिया और लगा चिल्लाने। जितना पोंछा जाए उतना जले और वह उतना और रोए। गर्मियों में उसे नंगा बैठा चुसुआ आम चेंप निकाल कर पकड़ा दिया जाता था। वह खाता और उसका पूरा शरीर आम रस से नहाया रहता। अक्सर शाम को आमरस और पराठे खाए जाते। एक आना सेर आम मिलता था, चार-पाँच सेर ले आते थे। पहले बाल्टी में पानी में रख दिया जाता फ़िर रस निचोड़ कर उसमे यदि जरूरत होती तो चीनी मिलाई जाती। आम की कुल्फ़ी घर में जमाई जाती। जो भी बनता पास-पड़ौस में बाँट कर खाया जाता। सर्दियों में रसिओर बनता। गन्ने के ताजे रस की खीर। इसे गर्मागरम खाया जाता बासी और ठंडा होने पर दूध डाल कर खाया जाता। और सर्दियों में बनती मटर की कचौड़ियाँ, टमाटर की मीठी चटनी।
एक बार हम तीज-त्योहार पर छुट्टियों में या तो नानाजी के यहाँ बनारस जाते या फ़िर बाबा-दादी के यहाँ गोरखपुर। जब हम वहाँ जाते तो बहन चाचा-बुआ की सुना-सुनी पिताजी को भैया कहती और माताजी को भाभी। एक बार हम गए तो उसने मुझसे कहा, ‘मुन्नी खेलने चलोगी?’ मेरे तन-बदन में आग लग गई। मुन्नी कह रही है जबकि कहना चाहिए ‘जीजी’। मैंने घूर कर देखा। बाद में उसने मुझे सदा जीजी कहा। बाकी सब बड़ी जीजी कहते, वह छोटी जीजी थी। मेरी यह बहन भी इसी साल गई।
बनारस में नानाजी का घर गायघाट गहनाबाई के बाड़ा में था। मौसी की सुसराल बड़ा गणेश पर। नानाजी आर्यसमाजी थे, गुरुकुल काँगड़ी के मंतकी। मौसी का घर पक्का सनातनी है। राधा-कृष्ण की सुबह-शाम आरती करने, छूआछूत का कड़ाई से पालन करने वाला। मौसेरा भाई और मैं गायघाट से हाथ पकड़ कर दौड़ते हुए बड़ा गणेश चले जाते। नानीजी की पड़ौसिन को मैं मौसी कहती थी। वे मुझे बहुत प्यार करती थीं। मैं एक नम्बर की चटोरिन ठहरी। आज भी हूँ, अब कई चीजें खाना मना है। ये मौसी जब दूध गरम करती मैं टुकुर-टुकुर देखती, वे मेरी आदत जानती थीं। दूध से उतार कर खूब गाढ़ी मलाई मेरी हथेली पर रख देती, उस पर चीनी या बूरा डाल देती और मैं चट कर जाती। एकाध दिन माताजी ने कुछ नहीं कहा पर जब रोज होने लगा तो उन्होंने मुझे बरजा। मैं भला क्यों सुनने लगी। अगले दिन फ़िर उनके चूल्हे के सामने थी, मजे में मलाई खा कर लौटी। माताजी बहुत गुस्से में थीं। उन्होंने चिमटा गरम कर मेरी हथेली दाग दी, कहा, ‘और जाएगी मलाई खाने?’ इन मौसीजी का एक दिन अपने पति से झगड़ा हुआ। बाद में मुझे समझ में आया झगड़े का कारण दूसरी औरत थी। झगड़ा बढ़ा और उसी समय पति ऐंठ गए और बस उनका राम-नाम सत्त हो गया। फ़िर पूरे बाड़े में खूब रोना-पीटना हुआ। यह उन कुछ पहली मौत में से एक थी जो मैंने देखी। पर तब उसका खास असर हुआ ऐसा अब याद नहीं है।

इटावा के बकेवर में हम घटना पर रहते थे। स्थान का नाम घटना क्यों था, वहाँ कौन-सी घटना घटी, मुझे नहीं मालूम। तब यह सब खुर्दबीन, उखड़पेंच दिमाग में नहीं आते थे। यह स्थान गाँव में काफ़ी ऊँचाई पर था। घर में खारे पानी का काफ़ी गहरा (चालीस हाथ) कूँआ था। पीने का पानी पिताजी के ऑफ़िस का चपरासी देव बहादुर दूर से लाता था। केवल हमारा घर पक्का और दोमंजिला था। बगल में एक दीक्षित परिवार रहता था। गाँव का रहवास जाति अनुसार था। हमारे घर की दूसरी ओर एक खंडहर था। दीक्षितजी की पहली पत्नी से एक बेटा और एक बेटी थी। पत्नी के मरने के बाद उन्होंने अपनी साली से शादी की। साली उनके बेटे-बेटी की हमउम्र थीं, थोड़ी बड़ी रही होंगी। बच्चे उन्हें माँ कहने से कतराते थे। बेटा अक्सर बाहर रहता लेकिन बेटी से बराबर उनकी खटपट होती रहती। दीक्षितजी की एक विधवा बहन भी उन्हीं के घर में रहती थीं, जगत बुआ। उनकी पत्नी को सब लोग मलकिनी कहते थे। मलकिनी की संतान जीवित नहीं रहती थी और हर बार लड़का होता था। हर बार मरा हुआ। हम लोग आर्यसमाजी थे। पिताजी हर इतवार सुबह हवन करते, रोज शाम को मंत्र पढ़े जाते लेकिन हर पूर्णिमा को हमारे घर में सत्यनारायण की कथा होती थी। दीक्षित जी कथा कहने आते थे।
घटना पर एक टूटा-फ़ूटा मंदिर था। पता नहीं कौन रोज शाम को उस मंदिर में दिया जलाया करता था। वहीं पेड़ की छाया में कुछ आदमी चौपड़ खेला करते थे। हमारे घर में कहा जाता था जो चौपड़ खेलता है वह चौपट हो जाता है, कहा जाता ताश करे नाश। हम शतरंज और लूडो खेलते थे। उन दिनों हवाई जहाज एक अजूबा हुआ करता था। मुझे पहली बार इसी घर की छत पर खड़े हो कर हवाई जहाज देखने की याद है। हवाई जहाज की आवाज सुन कर पूरा गाँव अपने-अपने घर से बाहर निकल आया था और देर तक लोग हवाई जहाज के क्षितिज में विलीन होने के बाद भी उस दिशा में देखते रह गए थे।
यहीं पहली बार पिताजी का एक चपरासी स्कूल में मेरा नाम लिखवा आया। लेकिन दो-तीन दिन बाद पिताजी ने देखा वहाँ जमीन पर बैठना होता है, और कई बच्चों की नाक बह रही है, जिसे वे उल्टी हथेली से पोंछ रहे हैं। उसके बाद मुझे स्कूल नहीं भेजा गया और इस तरह मेरे पहले विद्यालयी जीवन की इतिश्री हुई। यहीं मेरी सहेली सूरज ने मुझे बताया था जब फ़ोड़ा हो जाए या चोट लग जाए तो उस पर पाउडर (टेल्कम) लगाना चाहिए। पता नहीं अब कहाँ होगी सूरज? होगी भी या नहीं। इसी तरह देवबंद में स्कूल जाने के साथी दो लड़के थे एक का नाम याद है विमल। उसके पिताजी होमियोपैथ डॉक्टर थे। जाने कहाँ होंगे ये लोग? कैसा जीवन बिताया होगा इन लोगों ने। कई बार मन करता है इन जगहों पर फ़िर से जाने का। क्या मन का सोचा सब होता है? मेरे बचपन का यह उजला पक्ष है जाहिर है एक श्याम पक्ष भी है।

डॉ. विजय शर्मा
वरिष्ठ साहित्यकार
जमशेदपुर, झारखंड