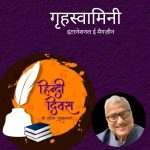क्षितिज की ओर
मुग्ध हो कर देख रहा हूं
और बह रहा हूं
अस्तित्व की बाढ़ में
तेरी अविजित मुस्कान
इधर झनझनाती तंत्रियों में शुरू
सामूहिक गान।
तू झुलसा रही मेरे अहं को
मेरी दुर्बलता को
उमड़ रहा न जाने क्या
झुकती नज़र, कभी उठती नज़र
पर इसके माने क्या?
फुलवारी कुछ सिमट गई है
और थोड़ी-सी आहट से
कांपने लगी है
तूफ़ान के अंदेशे ने
क्या क्या जुर्म किए
मजबूर हो गया
खुद को सहने के लिये
क्योंकि बिच्छू ने मारा डंक
पावक चेतना पर
एक एक क्षण का बोझ
वाचाल तन-मन
पर जिह्वा ने एक न कही
नीरवता खाये जा रही
तेरी चुप्पी में
मैं चढ रहा हाँफते-हाँफते हिमालय
फिर गगन भी दूर नहीं
तेरा अव्यक्त भाव
और मैं था पिंजरे में बंद पक्षी
लेकिन जा रहा हूं क्षितिज की ओर!

हरिहर झा
मेलबॉर्न ,ऑस्ट्रेलिया