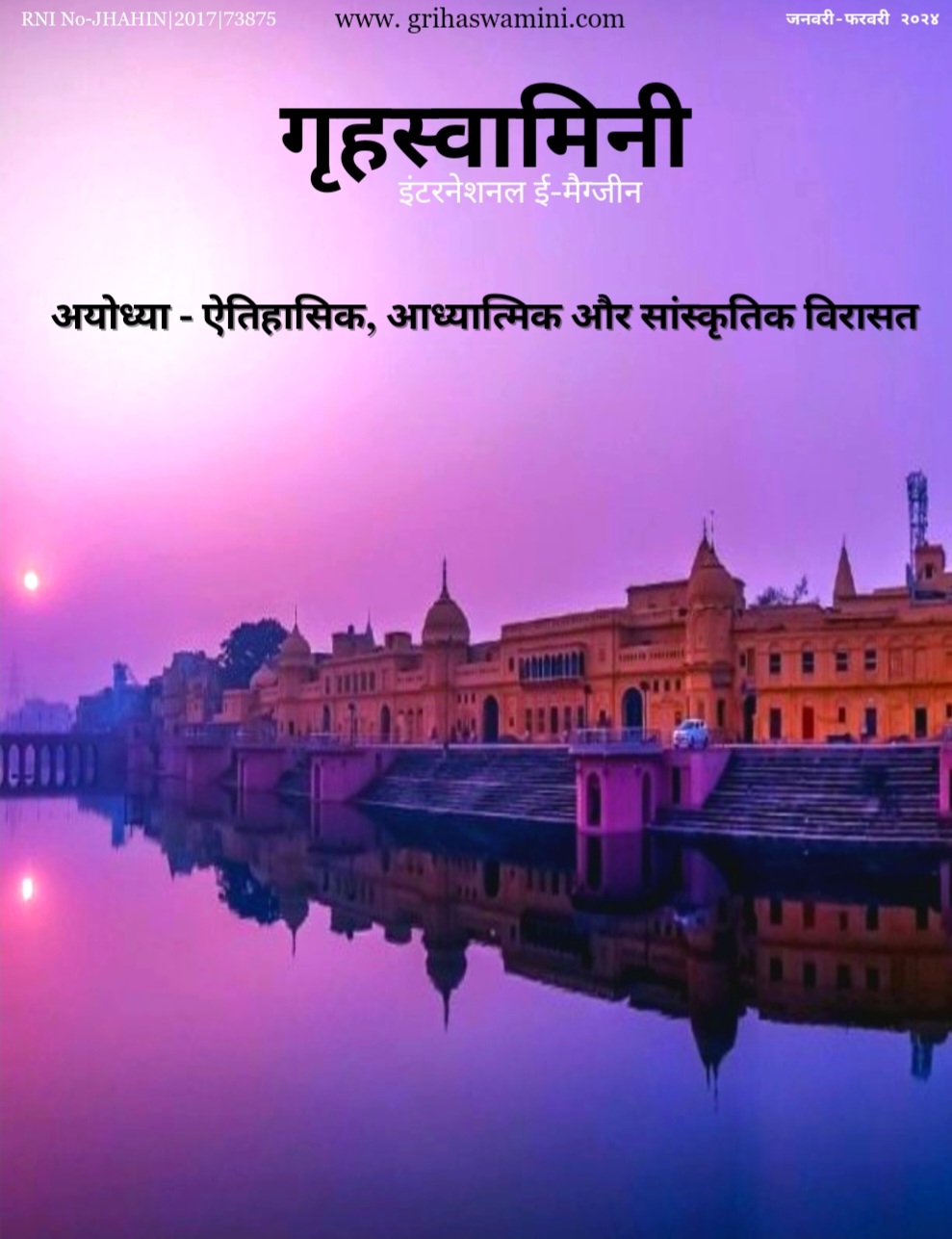पचास की दहलीज पार करती औरतें
ये पचास की दहलीज पार करती औरतें
वाकई बहुत विचित्र होती हैं,
एकदम समझ से परे..
कई बार लगता मानों समेटे हों
कितने गहरे राज अपने भीतर
बिल्कुल सीप में मोती के मानिंद..
दबाए रखती हैं कितने एहसास
चेहरे पर बढ़ती झुर्रियों में और
फिर उन्हें में मेकअप की परत में
छुपाकर मुस्कुरा देती हैं, मानो
कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो..
हासिल हुई खुशियों के दामन में
समेट लेती हैं कितने ही अश्क
जो बरसों बहते रहे नैनों से
वजह बेवजह कहीं भी, कभी भी..
आंगन की अर्गनी पे टाँगती हैं
चुनर के साथ साथ अपने सोए अरमाँ
जानती है वह कि ओढ़नी के साथ ही
बँधी रहेंगी ये अधूरी ख्वाहिशें भी..
स्वेटर के फंदों में उलझ कर अक्सर
सुलझाने लगती हैं जीवन की समस्याओं को
रंग बिरंगे फूल पत्तियों को उकेरती हुई
अपने ही मनोभावों को नया रूप देने लगती हैं..
कमजोर पड़ती याद्दाश्त के चलते
अक्सर फ्रिज में रखने चली जाती हैं
कुछ धुले हुए कपड़े अलमारी समझ
जाने क्यों जमा देना चाहती है वह
उनके साथ जुड़ी हुए अपनी यादों को..
अक्सर किटी पार्टियों में कहकहों में
उड़ा देती हैं अपने दर्द को बेसबब
जिंदगी के इस सांध्यकाल को जैसे
बाँधकर रख लेना चाहती हों कुछ खुशनुमा पलों के साथ..
पर यहीं पचास की दहलीज पार करती औरतें
वक्त की इस धुंधलाती चादर से निकाल पैर
अक्सर लड़ जाती हैं खुद के मिटते वजूद की खातिर
अब परवाह नहीं करती उन तानों और उलाहनों का
जिन्हें सुनते सहते जीवन के पाँच दशक बिता दिए..
नहीं घबराती अब रेल बसों की बढ़ती भीड़ से
क्योंकि जीवन के संघर्षों से जिस्म को ढाल चुकी होती
अहिल्या की तरह एक प्रस्तर प्रतिमा में
जिन पर घूरती वासनामय निगाहें नहीं टिक पाती..
तन्हाइयों से गहरा नाता जोड़ने की कुवद
शायद शारीरिक परिवर्तन को स्वीकार करते करते
भीड़भाड़ वाले माहौल से कतराने लगती हैं
क्योंकि ये बदलाव उनके अंतस को शून्य में धकेल देते हैं कभी कभी..
घर, परिवार, समाज से इतर भी जीना है
यह बात जाने कब, कैसे मन के भीतर पैठ गई
इसी लिए तो
अब अपने अस्तित्व की पहचान की खातिर
ढूँढने लगती हैं कोई नई राह, मंजिल का जिसकी कोई अता पता नहीं…
सीमा भाटिया
वरिष्ठ साहित्यकार